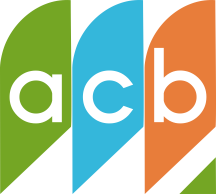गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण इकाई है, जो शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ औपचारिक संरेखण से बचकर रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की मांग करने वाले राज्यों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। विऔपनिवेशीकरण युग से उभरते हुए, NAM ने मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता का दावा करने, महाशक्ति आधिपत्य का विरोध करने और अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू, NAM की अवधारणा और स्थापना, इसके सिद्धांतों को आकार देने और भारत को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में स्थापित करने में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। यह प्रतिक्रिया ऐतिहासिक संदर्भ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत पर आधारित, नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ NAM की उत्पत्ति, सिद्धांतों, विकास और चुनौतियों का एक विस्तृत अकादमिक विश्लेषण प्रदान करती है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन: उत्पत्ति और संदर्भ
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी, लेकिन इसकी वैचारिक नींव 1955 में इंडोनेशिया में हुए बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी। बांडुंग सम्मेलन, जिसमें 29 एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भाग लिया था, द्विध्रुवीय शीत युद्ध की प्रतिक्रिया था, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सैन्य गठबंधनों (जैसे, नाटो और वारसॉ संधि) और आर्थिक प्रभाव के माध्यम से वैश्विक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। औपनिवेशिक शासन से उभरे नए स्वतंत्र राज्यों पर अपनी संप्रभुता और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को खतरे में डालते हुए, एक महाशक्ति समूह के साथ जुड़ने का दबाव था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक तीसरा रास्ता सुझाया, जिसमें स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद-विरोध और विकासशील देशों के बीच एकजुटता पर ज़ोर दिया गया।
शीत युद्ध की वैचारिक और सैन्य प्रतिद्वंद्विता ने इन राज्यों के लिए एक अनिश्चित वातावरण तैयार कर दिया। कोरियाई युद्ध (1950-1953), स्वेज संकट (1956), और चल रहे औपनिवेशिक संघर्षों ने बाहरी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए एक सामूहिक आवाज़ की आवश्यकता को रेखांकित किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन पूर्व की पहलों, जैसे 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन और 1955 में अफ्रीकी-एशियाई जन एकजुटता सम्मेलन, से भी प्रभावित था, जिसने उपनिवेशवाद के विरुद्ध क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा दिया।
संस्थापक और प्रमुख व्यक्ति
युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज़ टीटो की मेजबानी में बेलग्रेड सम्मेलन ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया, जिसके 25 संस्थापक सदस्य थे। प्रमुख नेताओं में शामिल थे:
- जवाहरलाल नेहरू (भारत): राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सक्रिय रुख के रूप में गुटनिरपेक्षता की वकालत की।
- गमाल अब्देल नासिर (मिस्र): साम्राज्यवाद-विरोध और अरब राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया।
- क्वामे नक्रूमा (घाना): अफ्रीकी एकता और उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- सुकर्णो (इंडोनेशिया): एशियाई-अफ्रीकी एकजुटता का समर्थन किया।
- जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया): समाजवादी और गुटनिरपेक्ष आदर्शों को जोड़ते हुए एक यूरोपीय परिप्रेक्ष्य प्रदान किया।
2025 तक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 120 हो जाएगी, जो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 17 पर्यवेक्षक देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद देशों का सबसे बड़ा समूह बना हुआ है।
सिद्धांत और उद्देश्य
एनएएम के मूल सिद्धांत, बेलग्रेड (1961) में व्यक्त किए गए और हवाना घोषणा (1979) द्वारा सुदृढ़ किए गए, उत्तर-औपनिवेशिक और आधिपत्य-विरोधी आदर्शों में निहित हैं:
- संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान: बाहरी हस्तक्षेप के बिना राज्यों के आत्मनिर्णय के अधिकार को कायम रखना।
- उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध: विउपनिवेशीकरण का समर्थन करना और नव-औपनिवेशिक आर्थिक प्रभुत्व का विरोध करना।
- महाशक्ति ब्लॉकों के साथ गुटनिरपेक्षतामहाशक्तियों से जुड़े सैन्य गठबंधनों में भागीदारी से बचना।
- शांतिपूर्ण सह - अस्तित्वपंचशील सिद्धांतों (परस्पर सम्मान, अहिंसा, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व) से प्रेरित, जिसे 1954 में भारत और चीन द्वारा सह-लिखित किया गया था।
- आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना: समतापूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रणालियों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग की वकालत करना।
- बहुपक्षवाद के लिए समर्थनवैश्विक शासन के लिए एक मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना।
इन सिद्धांतों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक प्रति-आधिपत्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसने द्विध्रुवीय शक्ति संरचना को चुनौती दी तथा विकासशील देशों की आवाज को बुलंद किया।
विकास और समकालीन प्रासंगिकता
शीत युद्ध काल (1961-1991)
शीत युद्ध के दौरान, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उपनिवेशवाद-विरोध, निरस्त्रीकरण और आर्थिक समानता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:
- अफ्रीका में मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करना (उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी संघर्ष)।
- वैश्विक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (एनआईईओ) की वकालत करना।
- वियतनाम युद्ध, अरब-इजरायल संघर्ष और क्यूबा की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना।
हालांकि, एनएएम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आंतरिक विभाजन (जैसे, सोवियत समर्थक और पश्चिमी समर्थक सदस्यों के बीच) और बाध्यकारी प्राधिकार या स्थायी सचिवालय की कमी के कारण अप्रभावी होने के आरोप शामिल थे।
शीत युद्धोत्तर युग (1991–2025)
1991 में सोवियत संघ के पतन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाले एकध्रुवीय विश्व में NAM की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए। हालाँकि, NAM ने नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करके खुद को ढाल लिया:
- वैश्वीकरण और आर्थिक असमानतानवउदारवादी नीतियों की आलोचना करना तथा निष्पक्ष व्यापार और ऋण राहत की वकालत करना।
- उभरते मुद्देजलवायु परिवर्तन, डिजिटल संप्रभुता और वैक्सीन इक्विटी (उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के दौरान) को संबोधित करना।
- एकतरफावाद का प्रतिरोध: ईरान, वेनेजुएला और क्यूबा जैसे देशों पर प्रतिबंधों का विरोध, जैसा कि 2024 कंपाला शिखर सम्मेलन में उजागर किया गया था।
2025 तक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वैश्विक दक्षिण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना रहेगा, जो अमेरिका, चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुधारों (जैसे, सुरक्षा परिषद का विस्तार) और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करेगा। इसकी घूर्णनशील अध्यक्षता (2024-2025 में युगांडा) विविध नेतृत्व सुनिश्चित करती है, हालाँकि स्थायी सचिवालय का अभाव संस्थागत निरंतरता को सीमित करता है।
चुनौतियां
एनएएम की प्रभावशीलता निम्नलिखित कारणों से बाधित है:
- विविध सदस्यताराजतंत्र, लोकतंत्र और सत्तावादी शासन को शामिल करते हुए, परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं को जन्म देना।
- आर्थिक निर्भरताकई सदस्य प्रमुख शक्तियों से व्यापार या सहायता पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता कमजोर होती है।
- कथित अप्रासंगिकताआलोचकों का तर्क है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शीत युद्ध से उत्पत्ति के कारण यह साइबर युद्ध या जलवायु वित्त जैसे समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए कम उपयुक्त है।
- सामंजस्य की कमीअसहमति, जैसे कि भारत के अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध या मिस्र का पश्चिमी शक्तियों के साथ गठबंधन, एकता को चुनौती देते हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद, NAM का आकार और नैतिक अधिकार इसे वैश्विक दक्षिण के हितों की वकालत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाते हैं।
NAM में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका
बौद्धिक आधार
जवाहरलाल नेहरू (1889-1964), 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री, गुटनिरपेक्षता के प्रमुख निर्माता थे। यह नीति भारत के औपनिवेशिक इतिहास और उत्तर-औपनिवेशिक विश्व व्यवस्था के उनके दृष्टिकोण पर आधारित थी। नेहरू के बौद्धिक ढाँचे में यथार्थवाद और आदर्शवाद का सम्मिश्रण था।
- यथार्थवादभारत की सीमित सैन्य और आर्थिक शक्ति को स्वीकार करते हुए, नेहरू ने महाशक्ति संघर्षों में उलझने से बचने के लिए रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की।
- आदर्शवादगांधीवादी सिद्धांतों और समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर, उन्होंने समानता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और साम्राज्यवाद-विरोध पर आधारित विश्व की कल्पना की।
नेहरू की विदेश नीति ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत के संघर्ष से प्रभावित थी, जिसने संप्रभुता और आत्मनिर्णय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने गुटनिरपेक्षता को एक सक्रिय रणनीति के रूप में देखा, न कि निष्क्रिय तटस्थता के रूप में, जिससे भारत को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए दोनों महाशक्तियों के साथ जुड़ने का अवसर मिला।
NAM में प्रमुख योगदान
1. बांडुंग सम्मेलन (1955):
- बांडुंग सम्मेलन में नेहरू एक अग्रणी व्यक्ति थे, जहाँ उन्होंने एशियाई-अफ्रीकी एकजुटता और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। चीन के साथ मूल रूप से विकसित पंचशील सिद्धांतों की उनकी वकालत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के चरित्र का आधार बन गई।
- उन्होंने भारत को एशिया और अफ्रीका के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित किया तथा साम्राज्यवाद के प्रति सामूहिक प्रतिरोध और आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया।
- बांडुंग में नेहरू के भाषणों में नैतिक कूटनीति पर जोर दिया गया तथा राष्ट्रों से सैन्य गुटों को अस्वीकार करने तथा विकास पर ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया गया।
2. एनएएम का गठन (1961):
- बेलग्रेड सम्मेलन में, नेहरू ने टीटो, नासिर, नक्रूमा और सुकर्णो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने तर्क दिया कि गुटनिरपेक्षता अलगाववाद नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने की एक गतिशील नीति है।
- नेहरू के समावेशिता पर जोर देने से यह सुनिश्चित हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने राजनीतिक व्यवस्था की परवाह किए बिना विविध राज्यों का स्वागत किया, जिससे एक व्यापक गठबंधन को बढ़ावा मिला।
3. नैतिक और कूटनीतिक नेतृत्व:
- नेहरू ने परमाणु निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद-विरोध और आर्थिक समानता की वकालत करते हुए, भारत को वैश्विक मामलों में एक नैतिक आवाज़ के रूप में स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य मंचों पर उनके नेतृत्व ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रभाव को बढ़ाया।
- उन्होंने कोरियाई युद्ध जैसे संघर्षों में मध्यस्थता की, जिससे शांति स्थापना की रणनीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
- नेहरू के दृष्टिकोण ने अन्य नेताओं को प्रेरित किया, विशेष रूप से अफ्रीका में, जहां एनक्रुमा जैसे लोगों ने उनके विचारों से प्रेरणा लेकर अपनी उपनिवेश-विरोधी नीतियां बनाईं।
4. पंचशील और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व:
- नेहरू ने 1954 में चीन के झोउ एनलाई के साथ मिलकर पंचशील सिद्धांतों का निर्माण किया, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए एक मार्गदर्शक ढाँचा बन गया। इन सिद्धांतों ने पारस्परिक सम्मान और अहस्तक्षेप पर ज़ोर दिया, जिससे शीत युद्ध के टकराव का एक कूटनीतिक विकल्प सामने आया।
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के बावजूद, जिसने नेहरू की पंचशील में आस्था को चुनौती दी, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता NAM की विचारधारा की आधारशिला बनी रही।
नेहरू की भूमिका की आलोचना
यद्यपि नेहरू का योगदान महान था, फिर भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा:
- आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकतामाइकल ब्रेचर जैसे विद्वानों का तर्क है कि नेहरू की आदर्शवादी दृष्टि ने विविध राष्ट्रों को एकजुट करने की व्यावहारिक चुनौतियों को कम करके आंका। चीन के पंचशील के प्रति उनके विश्वास को 1962 के युद्ध ने हिला दिया, जिसने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से निपटने में गुटनिरपेक्षता की सीमाओं को उजागर कर दिया।
- भारत की सीमित क्षमताएपी राणा जैसे आलोचकों का मानना है कि भारत के पास गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावी नेतृत्व करने के लिए आर्थिक या सैन्य शक्ति का अभाव है, तथा वह भौतिक प्रभाव के बजाय नैतिक अधिकार पर निर्भर है।
- गुटनिरपेक्षता में अस्पष्टताएँनेहरू के दोनों महाशक्तियों के साथ जुड़ाव (जैसे, औद्योगीकरण के लिए सोवियत सहायता स्वीकार करना) ने कुछ लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या गुटनिरपेक्षता वास्तव में गैर-पक्षपाती थी। यथार्थवादियों का तर्क है कि यह सख्त तटस्थता के बजाय व्यावहारिक संतुलन को दर्शाता है।
परंपरा
नेहरू का गुटनिरपेक्षता का दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों में अक्षुण्ण है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलनों में भारत का नेतृत्व, वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर उसकी वकालत, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों में उसकी भूमिका, नेहरू के दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ज़ोर को दर्शाती है। उनका बौद्धिक ढाँचा आज भी बहुध्रुवीय विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता पर बहस को प्रेरित करता है।
शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य: सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नेहरू की भूमिका का विश्लेषण कई सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है:
- उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांतविजय प्रसाद जैसे विद्वान गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती देने और निम्न वर्गीय राष्ट्रों के लिए एक "तीसरा स्थान" बनाने की एक उत्तर-औपनिवेशिक परियोजना मानते हैं। नेहरू का नेतृत्व इसी ढाँचे के अनुरूप है, जिसमें आत्मनिर्णय और साम्राज्यवाद-विरोध पर ज़ोर दिया गया है।
- मध्य-शक्ति कूटनीतिएंड्रयू कूपर की मध्य शक्तियों की अवधारणा नेहरू के शासनकाल में भारत पर लागू होती है, जिसने सीमित भौतिक शक्ति के बावजूद अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इस्तेमाल किया। नेहरू की कूटनीति ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए मृदु शक्ति—नैतिक अधिकार और बहुपक्षवाद—का लाभ उठाया।
- निर्भरता सिद्धांतआंद्रे गुंडर फ्रैंक जैसे आलोचकों का तर्क है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आर्थिक लक्ष्य पश्चिमी बाज़ारों और सहायता पर सदस्यों की निर्भरता के कारण सीमित थे। नेहरू के आत्मनिर्भरता (स्वदेशी) के प्रयास ने इसका प्रतिकार करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें संरचनात्मक सीमाएँ थीं।
- यथार्थवाद बनाम आदर्शवादनेहरू की गुटनिरपेक्षता ने यथार्थवादी रणनीतियों (सैन्य उलझनों से बचना) को आदर्शवादी लक्ष्यों (वैश्विक शांति और समानता) के साथ संतुलित किया। यथार्थवादी इसे भोलापन मानते हैं, जबकि रचनावादी इसे शीत युद्ध की शक्ति संरचना के लिए एक मानक चुनौती मानते हैं।
समकालीन प्रासंगिकता (2025)
2025 तक, NAM वैश्विक दक्षिण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना रहेगा, जो निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देगा:
- डिजिटल संप्रभुताप्रौद्योगिकी तक समान पहुंच की वकालत करना और गलत सूचना का मुकाबला करना।
- जलवायु न्यायजलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देना, जैसा कि 2024 कंपाला शिखर सम्मेलन में जोर दिया गया था।
- प्रतिबंधों का प्रतिरोधईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के खिलाफ एकतरफा कदमों की आलोचना करना।
- संयुक्त राष्ट्र सुधार: अधिक प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा परिषद की वकालत करना।
भारत अपनी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत को रणनीतिक साझेदारियों (जैसे, क्वाड, ब्रिक्स) के साथ संतुलित करते हुए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नेहरू के संप्रभुता और बहुपक्षवाद के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि भारत अमेरिका, चीन और रूस के बीच तनाव से जूझ रहा है।
निष्कर्ष
गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा, जिसने विकासशील देशों को महाशक्तियों के प्रभुत्व का विरोध करने और संप्रभुता, शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक और कूटनीतिक नेतृत्व ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से गुटनिरपेक्षता, पंचशील और दक्षिण-दक्षिण एकजुटता के उनके समर्थन के माध्यम से। जहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक बहुध्रुवीय विश्व में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसकी स्थायी प्रासंगिकता वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बुलंद करने की इसकी क्षमता में निहित है। आदर्शवाद और व्यावहारिकता का मिश्रण, नेहरू की विरासत, भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मिशन को प्रभावित करती रही है, जिसने उन्हें उत्तर-औपनिवेशिक वैश्विक शासन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया है।