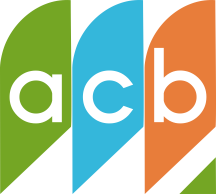1960 में सिंधु जल संधि (IWT) पर हस्ताक्षर करके जवाहरलाल नेहरू "गलत" थे या नहीं, यह इस निर्णय के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए गए परिप्रेक्ष्य और मानदंडों पर निर्भर करता है। विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच आवंटित किया। इसने भारत को पूर्वी नदियों (सतलुज, व्यास, रावी) पर और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर नियंत्रण दिया, साथ ही भारत द्वारा जलविद्युत जैसे गैर-उपभोग्य उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए। यहाँ तर्कों पर एक संतुलित नज़र डाली गई है:
नेहरू को “गलत” बताने वाले तर्क
- सामरिक संसाधनों की रियायतआलोचकों का तर्क है कि ऊपरी तटवर्ती राज्य होने के नाते, भारत ने पश्चिमी नदियों पर बहुत अधिक नियंत्रण छोड़ दिया, जो सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह का लगभग 801 टन (TP3T) हिस्सा हैं। इससे भारत की इन नदियों का सिंचाई, जलविद्युत या रणनीतिक लाभ के लिए, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में, पूर्ण उपयोग करने की क्षमता सीमित हो गई।
- दीर्घकालिक बाधाएँयह संधि भारत की जल संग्रहण बाँध बनाने या पश्चिमी नदियों के प्रवाह में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता को सीमित करती है, जिसे कुछ लोग जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और ऊर्जा आवश्यकताओं जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने में बाधा मानते हैं। उदाहरण के लिए, भारत पश्चिमी नदियों पर केवल रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएँ ही बना सकता है, जो जल संग्रहण के लिए कम कुशल हैं।
- सुरक्षा चिंताएंपाकिस्तान के साथ लगातार चल रहे तनाव को देखते हुए, कुछ आलोचकों का मानना है कि नेहरू ने एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करके नासमझी की, जो भारत की जल को भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को सीमित करती है। उनका तर्क है कि जल का इस्तेमाल पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता था, खासकर संघर्ष के समय में।
- घरेलू राजनीतिक प्रतिक्रियाभारत में, खासकर जम्मू-कश्मीर में, इस संधि को लेकर नाराजगी है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि यह क्षेत्र की विकास संभावनाओं को सीमित करता है, क्योंकि भारत बिजली या कृषि के लिए चिनाब और झेलम नदियों का पूरा दोहन नहीं कर सकता।
नेहरू के निर्णय के समर्थन में तर्क
- कूटनीतिक आवश्यकताउस समय, भारत और पाकिस्तान 1947 के विभाजन और युद्ध से उबर रहे थे। इस संधि को एक महत्वपूर्ण साझा संसाधन पर तनाव कम करने के एक उपाय के रूप में देखा गया था। नेहरू क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देते थे, और यह संधि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक दुर्लभ उदाहरण थी।
- अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिष्ठाविश्व बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस पर हस्ताक्षर करने से भारत की छवि एक ज़िम्मेदार और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के प्रति प्रतिबद्ध वैश्विक शक्ति के रूप में मज़बूत हुई। इस संधि को अस्वीकार करने से वैश्विक संस्थाओं के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो सकते थे।
- निष्पक्ष आवंटनजहाँ पाकिस्तान को जल का बड़ा हिस्सा मिला, वहीं भारत को पूर्वी नदियों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त हुआ, जो पंजाब और हरियाणा में उसकी तत्काल कृषि आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त था। सिंधु नदी प्रणाली पर पाकिस्तान की अधिक निर्भरता को देखते हुए, इस संधि को एक संतुलित समझौते के रूप में देखा गया।
- संधि की स्थायित्वसिंधु जल संधि तीन युद्धों (1965, 1971, 1999) और अनेक संकटों से बचकर अपनी लचीलापन साबित कर चुकी है। इससे पता चलता है कि जल-बंटवारे को औपचारिक रूप देने के नेहरू के फैसले ने जल को लेकर होने वाले विवादों को रोकने में मदद की, जो तनाव को और बढ़ा सकते थे।
- आर्थिक फोकसनेहरू सरकार ने तीव्र औद्योगीकरण और कृषि आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। पूर्वी नदियों ने 1960 और 1970 के दशक में भारत की हरित क्रांति के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया, जिससे पता चलता है कि उस समय संधि ने भारत के विकास में कोई खास बाधा नहीं डाली।
प्रासंगिक विचार
- ऐतिहासिक संदर्भ: 1950 के दशक में, बड़े बांध या भंडारण परियोजनाएँ बनाने की भारत की तकनीकी और वित्तीय क्षमता सीमित थी। उस समय पश्चिमी नदियों पर प्रतिबंध उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि भारत के पास उनका पूर्ण दोहन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव था।
- पाकिस्तान की निर्भरतापाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि सिंधु नदी प्रणाली, खासकर पश्चिमी नदियों पर बहुत अधिक निर्भर थी। पाकिस्तान को पहुँच से वंचित करने से आर्थिक पतन या युद्ध हो सकता था, जिससे भारत बचना चाहता था।
- आधुनिक प्रासंगिकताआज आलोचक प्रायः इस संधि का मूल्यांकन समकालीन दृष्टिकोण से करते हैं तथा 1960 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, भारत की बढ़ती ऊर्जा और जल आवश्यकताओं के कारण संधि की कुछ सीमाएं अधिक स्पष्ट हो गई हैं।
निष्कर्ष
उस समय के भू-राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संदर्भ को देखते हुए, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने का नेहरू का निर्णय एक व्यावहारिक निर्णय था। इसने स्थिरता सुनिश्चित की, तत्काल संघर्ष को टाला और भारत की व्यापक विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप था। हालाँकि, आधुनिक दृष्टिकोण से, पश्चिमी नदियों के भारत के उपयोग पर संधि के प्रतिबंध अत्यधिक रियायती लग सकते हैं, खासकर भारत की बढ़ती ज़रूरतों और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए। यह नेहरू को "गलत" बनाता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अल्पकालिक कूटनीतिक लाभ और स्थिरता (जहाँ संधि सफल रही) को प्राथमिकता देते हैं या दीर्घकालिक रणनीतिक लचीलेपन (जहाँ इसकी सीमाएँ हैं) को।